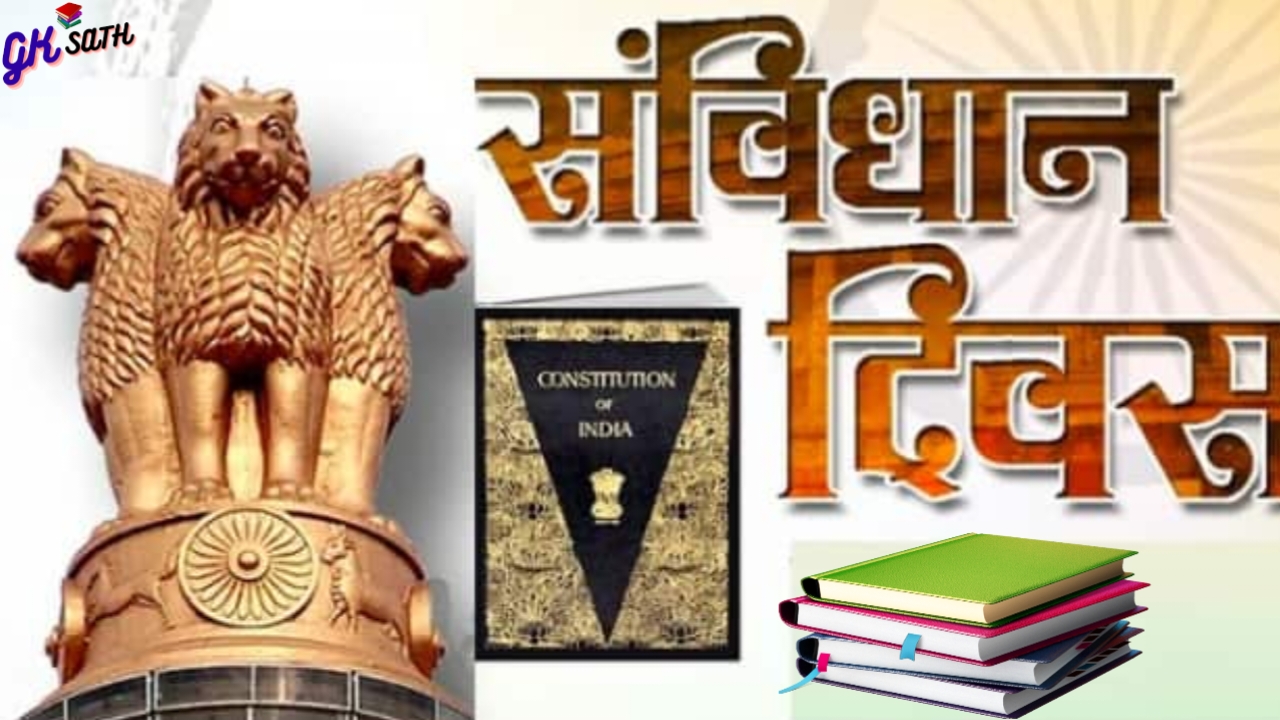भारतीय सविधान के विकास का संछिप्त इतिहास
भारतीय संविधान का विकास एक जटिल और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को स्थापित किया। आइए,

1.भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि:– भारतीय संविधान का निर्माण भारत की आज़ादी के बाद हुआ, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1858 में ब्रिटिश शासन की स्थापना से शुरू होती है। भारतीय नेताओं ने विभिन्न अधिनियमों के तहत अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की, जिनमें 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार और 1919 का मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधार प्रमुख थे। इन सुधारों ने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति रुचि जगाई।
2.स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का प्रारंभ:– 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, जो भारतीय संविधान के लिए एक प्रारंभिक मसौदा थी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी भारतीय संविधान की नींव रखने में सहायक बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के नेताओं ने एक संपूर्ण संविधान बनाने का सपना देखा जो एक स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके।
3. संविधान सभा का गठन:- 1946 में, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। संविधान सभा का कार्यभार भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर को इस सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण रहा।
4.संविधान सभा की बैठकें और चर्चा:– संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन तक संविधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। कुल 11 सत्रों में 165 बैठकों के दौरान, 2000 से अधिक संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इन बैठकों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई, जिससे एक संतुलित और समावेशी संविधान का निर्माण हो सका।
5.संविधान की मसौदा समिति:- संविधान की मसौदा समिति का गठन डॉ. भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति का मुख्य कार्य संविधान के प्रारूप को तैयार करना था। इस समिति ने 1948 में संविधान का मसौदा पेश किया, जिसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और उस पर विस्तार से चर्चा की गई।
6.संविधान का उदार स्वरूप:- भारतीय संविधान का स्वरूप उदार और प्रगतिशील है। यह विभिन्न समाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रमुखता दी गई है, जिनमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रमुख हैं। यह उदार स्वरूप भारतीय समाज की विविधता को समाहित करने में सहायक है।
7.भारत का संघीय ढांचा:- भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका संघीय ढांचा है। यह संघीयता केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन सुनिश्चित करता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से विभाजित किए गए हैं, जिससे संघीय ढांचे की मजबूती बनी रहती है और राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

8.धर्मनिरपेक्षता की विशेषता:- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता को अपनाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है और राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह विशेषता भारत जैसे बहुधर्मी समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
9.मौलिक अधिकार:– भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करते हैं। इनमें बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, और समानता का अधिकार प्रमुख हैं। यह अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।
10.मौलिक कर्तव्य:– संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझाना है। यह कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।
11.राज्य के नीति निर्देशक तत्व:– संविधान में राज्य के नीति निर्देशक त अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को समझाना है। यह कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हैं।
12.राज्य के नीति निर्देशक तत्व:– त्वों का उल्लेख है, जो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। राज्य इन तत्वों के अनुसार अपने नीतियों का निर्माण करता है ताकि समाज के सभी वर्गों का समावेश हो सके।
13.स्वतंत्र न्यायपालिका:–भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। यह न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर नज़र रखती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
14.न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार:– भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया है, जिसके तहत वह किसी भी कानून या सरकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। यह अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है।
15.संसदीय प्रणाली की स्थापना:- भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का सत्ता संचालन होता है। यह प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे अनुकूलित किया गया है। संसद में विधायी कार्यों के लिए दो सदनों की व्यवस्था की गई है – लोकसभा और राज्यसभा।
16.राष्ट्रपति की भूमिका:- संविधान में राष्ट्रपति को भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक और सेना का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया है। राष्ट्रपति का पद नाममात्र का है, लेकिन उनके पास संविधान की रक्षा और पालन कराने के महत्वपूर्ण अधिकार हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और उनकी भूमिका संविधान की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
17.संघीय न्यायालय की स्थापना:- भारतीय संविधान में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, जो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की व्याख्या करती है। यह न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने और संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघीय न्यायालय की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।
18.चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:- संविधान में चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना और इसे संविधान के अनुसार संचालित करना है। यह स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है कि चुनाव प्रक्रिया पर कोई बाहरी दबाव न हो और नागरिकों को अपने मताधिकार का स्वतंत्र उपयोग करने का अधिकार मिले।

19.संविधान संशोधन प्रक्रिया:- भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो संविधान में आवश्यक बदलाव करने के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होती है और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया संविधान को समयानुसार अनुकूलित करने में सहायक है।
20.संविधान की अनुकूलता:- भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसकी अनुकूलता है। संविधान में विभिन्न परिस्थितियों और समय के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। यह अनुकूलता संविधान को गतिशील और समयानुसार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से संविधान को बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
21.मूल संविधान और संशोधन:- भारतीय संविधान का मूल स्वरूप 1950 में लागू हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ, संविधान में विभिन्न संशोधन किए गए और नए अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो इसे समयानुसार अद्यतन बनाए रखते हैं और इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक बनाते हैं।
इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषता होती है
अगर इस पोस्ट की प्रश्न और उत्तर पढ़ने के लिए
CLECK बैटन से प्रेस करे